प्रयागराज महाकुम्भ नहीं, बौद्धों की ‘महादान भूमि’
By Tarunmitra
On
डॉ राजीव रत्न मौर्य
प्रयागराज में लगने वाले कुम्भ या महाकुम्भ को लेकर बौद्ध अनुयायियों के बीच पहले भी यह चर्चा होती रही है कि कुम्भ बौद्धों की परंपरा रही है लेकिन इस बार सोशल मीडिया के माध्यम से महान भाषा वैज्ञानिक राजेन्द्र प्रसाद सिंह और बौद्ध विद्वान राजेश चंद्रा जी ने जो बात तथ्यों के साथ बताई है वह बहुत हद तक लोगों के बीच पहुंची है कि कुम्भ बौद्धों की परंपरा रही है|
अभी हिंदुस्तान अखबार के 19 जनवरी 2025 के अंक में पत्रकार अभिषेक त्रिपाठी के बाई लाइन से छपी खबर “ह्वेनसांग ने 1400 साल पहले किया था कुम्भ स्नान” में अख़बार ने लिखा है, “सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत आये चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी महाकुम्भ स्थान पर पुण्यलाभ लिया था| ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृतांत में महाकुम्भ स्थल पर इन्सान ही नही पशु-पक्षियों में भी आस्था होने का जिक्र किया है| इसी अखबार में आगे लिखा है, “ महाकुम्भ के ऐतिहासिक पक्षों का अध्ययन कर रहे बी.एच.यू के प्राचीन संस्कृति और पुरातत्व विभाग के डॉ सचिन तिवारी कहते है कि 629 से 645 ईस्वी के दौरान सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने उत्तर भारत की यात्रा की थी और अपने यात्रा वृतांत में इस क्षेत्र का उल्लेख करते हुए सिर्फ दो नदियों गंगा और यमुना के बारे में ही लिखा है| डॉ सचिन तिवारी ने आगे बताया है कि ह्वेनसांग के विवरण में कुम्भ में आये लोगों को शिक्षाप्रेमी, विनम्र. सज्जन और सरल स्वाभाव का बताया है|
हालाँकि आधी-अधूरी ही सही लेकिन बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने सच को आगे बढाने में साहस दिखाया है कि सरस्वती नाम की कोई नदी का ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। डॉ सचिन तिवारी के अनुसार “ह्वेनसांग के विवरण में कुम्भ में आये लोगों को शिक्षाप्रेमी, विनम्र. सज्जन और सरल स्वाभाव का बताया है|” शिक्षाप्रेमी, विनम्रता. सज्जनता और सरल स्वाभाव आदि गुण तो सर्वाधिक बौद्ध भिक्षुओं में ही पाई जाती है| पुरुष नागा, महिला नागा, अघोरी, अखाड़ा ...और न जाने क्या-क्या नाम से कुम्भ/महाकुम्भ में कैंप किये हुए कुछ एक को छोड़कर लगभग सभी साधुओं के ब्यवहार में कही भी शिक्षाप्रेम, विनम्रता. सज्जनता और सरल स्वभाव आदि गुण नदारत दिखेंगे| कोई भी आस्थावान सभ्य हिदू परिवार इन्हें केवल दूर से ही प्रणाम करना चाहता है।
ह्वेनसांग के यात्रा विवरण यानि 7वीं सदी से पहले कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलेगा जो कुम्भ को ब्राह्मणी/हिन्दू संस्कृति का महापर्व बताता हो। बौद्धों की परंपरा, बौद्धों के बुद्ध विहार, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, कला, संस्कृति के केंद्र को समय-समय पर ब्राह्मणी संस्कृति के वाहकों और मुस्लिम आक्रान्ताओं ने नष्ट किया, यहाँ तक कि इंसानियत और मानवता का पाठ पढाने वाले निरीह बौद्ध भिक्षुओं का क़त्ल-ए-आम किया गया। अन्याय,अत्याचार शोषण, उत्पीडन जुल्म और ज्यादती के सहारे बौद्ध प्रतीकों, बिम्बों, उत्सवों, शिक्षा, कला, संस्कृति, बुद्ध विहारों और बुद्ध की मूर्तियों पर ब्राह्मणी संस्कृति के वाहकों ने कब्ज़ा कर लिया। आज सोशल मीडिया पर नित कोई न कोई विडियो वायरल हो रहा है जिसमे बुद्ध की मूर्तियों को हिदू देवी-देवता के रूप में पूजते दिखाया जाता है।
बी.एच.यू में पाली के विभागाध्यक्ष रहे बौद्ध विद्वान प्रोफेसर पंडित जगन्नाथ उपाध्याय ने अपनी किताब “बौद्ध संस्कृति बनाम ब्राह्मणी संस्कृति” में बहुत कुछ सच्चाई बयां किया है।यही नहीं प्रकांड महापंडित केदार नाथ पाण्डेय उर्फ़ राहुल सांकृत्यायन ने भी अपनी लिखित दर्जनों किताबों में बौद्ध संस्कृति पर हमले की दास्ताँ लिखी है।
भारत की धरती पर बहुत से धर्म, संप्रदाय, मजहब आदि का प्रादुर्भाव हुआ और बहुत से देवी-देवता भी हुए, ग्रंथों के अनुसार कुछ तो उड़ते भी थे लेकिन उड़कर भी अपने महान धर्म को दूसरे देश तक नहीं पहुंचा पाए और पैदल चलकर बुद्ध ने अपने प्रभाव से पूरे एशिया में अपने महान धम्म को पहुंचा दिया। देश की अपनी सीमा उसकी बाउंड्री होती है लेकिन धर्म की कोई बाउंड्री नहीं होती इसके बावजूद भी तथाकथित महान धर्म के अनुयाई यहीं भारत में ही अपना खून खौलाते रह गए उधर बुद्ध ने शांति और मानवता का सन्देश लेकर पूरी दुनिया में पहुँच गये। आज भी जब विदेश से किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भारत भूमि पर आता है तो भारत का कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो उसका स्वागत बुद्ध की मूर्ति देकर ही करता है। मेरा दावा है कि आज अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष भारतभूमि आता है और उसे महाकुम्भ ले जाया जाता है तो उसका भी स्वागत बुद्ध मूर्ति देकर ही करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के लोग भारत को बुद्ध भूमि के रूप में सम्मान देते हैं।
बौद्ध विद्वान् राजेश चंद्रा कहते है, “कुम्भ पर्व मौलिक रूप से एक बौद्ध पर्व है जो आज अपभ्रंशित स्वरूप में प्रचलन में दिखता है। यह पर्व मौलिक रूप से बौद्ध साधुओं को महादान देने का उत्सव था। दान पर्व जब सम्राट आयोजित कर रहे हों तो पात्र से अधिक अपात्र इकठ्ठा होने लगते हैं। यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि खोटा सिक्का असली मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। अगर किसी की जेब में एक नकली और दूसरी असली मुद्रा हो तो मुद्राधारक का पहला प्रयास रहता है कि नकली मुद्रा चला दी जाए। इस सरल से सिद्धांत के कारण नकली मुद्रा असली मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है। कुम्भ पर्व के साथ यही हुआ है। साधु से अधिक असाधु इकट्ठा होने लगे। श्रद्धा पर अंधश्रद्धा का प्रचार होने लगा। इतिहास पर मिथक हावी होने लगा। पराकाष्ठा यहाँ तक हो गयी कि कालान्तर में बौद्ध उपासक-उपासिकाओं तथा भिक्खुओं को बेदखल करने के लिए नग्न स्नान की परम्परा शुरू हुई, नतीजतन साधुओं की कुटियां 'अखाड़े' बन गये, इतिहास पर मिथक हावी हो गया। नग्न स्नान की परम्परा आज भी पूरी दुनिया में भारत का कितना अपमान कराती है कि हर भारत प्रेमी आहत महसूस करता है। नग्न स्नान की इस निर्लज्ज परम्परा ने एक महान आध्यात्मिक पर्व की आध्यात्मिकता और धार्मिकता को तार-तार कर दिया है और यह सब कुछ कथित धर्म के नाम पर हो रहा है, पूरे महिमामण्डन के साथ हो रहा है। किसी कथित धर्म प्रेमी में यह कहने का साहस नहीं है कि यह निर्लज्ज परम्परा कानूनन बन्द किया जाना चाहिए।
उज्जैन के कुम्भ की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। मराठा शासक रानोजी शिन्दे ने उज्जैन के एक स्थानीय उत्सव के लिए नासिक से साधुओं को आमंत्रित किया। सम्राट हर्षवर्धन का अनुकरण करते हुए रानोजी शिन्दे ने भी इस उत्सव को महादान का स्वरूप दिया। मराठा शासक रानोजी शिन्दे की पहल के परिणामस्वरूप कालान्तर में नासिक और उज्जैन के साधुओं की परस्पर प्रतिस्पर्धा ने क्षिप्रा के तट पर उज्जैन में और गोदावरी के तट पर नासिक में कथित कुम्भ की शुरुआत हुई। हरिद्वार के गंगा तट पर इसका विस्तार सम्राट हर्षवर्धन के समय ही हो चुका था और ब्रिटिश काल तक आते-आते यह एक स्थापित पर्व बन चुका था।
प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डी.पी.दूबे का कथन है: "किसी भी हिन्दू ग्रन्थ में प्रयाग मेला कुम्भ मेला के रूप में दर्ज़ नहीं है।"
'कुम्भ मेला' का पहला लिखित विवरण इस्लामी इतिहास ग्रंथों 'खुलासत-उल-तवारीख'(सन् 1695) और 'चाहर गुलशन'(सन् 1759) में मिलता है।
आधुनिक काल में 'कुम्भ मेला' का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रिटिश काल की एक आख्या, रिपोर्ट, में सन् 1868 में "Coomb fair" के रूप में मिलता है जो कि सन् 1870 में होना था। मैक्लियन के विवरणानुसार:" प्रयाग के प्रयागवाल ब्राह्मण ने सर्वप्रथम तीर्थ की महत्ता को महिमामण्डित करने के लिए माघ मेला को कुम्भ के रूप में आत्मसात किया।"
प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉ राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने यूट्युब चैनल पर बताते है, 7वीं सदी में ह्वेनसांग अपनी भारत यात्रा के क्रम में प्रयागराज भी गए। प्रयाग जिसे मुगलकाल में अल्लाहाबाद नाम दिया गया, उस समय बौद्ध केंद्र था। ह्वेनसांग ने लिखा है कि प्रयाग में दो संघाराम थे, हीनयानी बौद्ध वहा रहा करते थे और राजधानी के दक्षिण पश्चिम में चम्पक वन था और उस चम्पक वन में सम्राट असोक का बनाया हुआ बहुत ऊँचा धम्म स्तूप था जिसकी उंचाई उस समय कम से कम 100 फीट थी और नगर के पूरब में ‘महादान भूमि’ थी। आज जहाँ कुम्भ मेला का आयोजन होता है ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में उसे ‘महादान भूमि’ होने की बात लिखी है। महादान भूमि पर जो मेला का आयोजन होता था उसमे बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन महादान करने के लिए अपने पांच वर्षों का अर्जित खजाना दीन-दुखियों में बाँट दिया करते थे। महादान भूमि पर आयोजन की शुरूआत बुद्ध मूर्ति पर अलंकरण से होता था।
ह्वेनसांग ने यह भी लिखा है कि प्रयाग दो नदियों के किनारे है। तीसरी नदी सरस्वती का उल्लेख न तो ह्वेनसांग ने किया है और न ही बाल्मीकि और कालिदास ने ही किया है। बाल्मीकि और कालिदास ने बताया है कि प्रयाग में केवल दो ही नदिया थी एक गंगा और दूसरा यमुना। बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा है कि सरस्वती नदी उत्तर प्रदेश की सीमा में कभी थी ही नहीं। प्रश्न उठता है कि गंगा -जमुना के संगम को फिर त्रिवेणी क्यों कहा जाता है ? इसकी ब्याख्या भाषा बैज्ञानिक के रूप में किशोरी दास वाजपेयी करते हुए लिखते हैं, त्रिवेणी का मतलब तीन नदी नहीं होता। वेणी का अर्थ प्रवाह होता है इस प्रकार त्रिवेणी का मतलब तीन धाराओं का प्रवाह न कि तीन नदियाँ। त्रिवेणी तीन धाराएँ हैं एक गंगा की धारा, दूसरी यमुना की धारा और तीसरी गंगा और यमुना की संयुक्त धारा/प्रवाह, यह होता है त्रिवेणी का अर्थ।
इन ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में देखें तो आज का वर्तमान कुम्भ मौलिक रूप से बौद्धों के द्वारा स्थापित “महामोक्ष्य परिषद” जिसके द्वारा ‘महादान भूमि’ पर आयोजित होने वाले महादान का एक महापर्व है। समय की मांग तो यह है कि इस पर्व को भारत पर्व बना दिया जाए जहाँ समता-स्वतंत्रता-बन्धुता-न्याय का उत्सव हो क्योंकि यह भी दुनिया में एक अनुपम मिसाल है जहाँ बिना निमंत्रण के लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, विविध भारत एक दिखता है। यह भारत की एकता का पर्व भी बनाया जा सकता है। इसकी पहल हर भारत प्रेमी को करना चाहिए। इसकी मौलिक आध्यात्मिकता व धार्मिकता को संरक्षित करना हर भारत प्रेमी का नैतिक कर्तव्य है। जिस दिन यह पर्व अपनी मौलिक आध्यात्मिकता को पुनः उपलब्ध होगा भारत फिर विश्व गुरू होगा।
-डॉ राजीव रत्न मौर्य पूर्व संपादक - अम्बेडकर टुडे
About The Author

‘तरुणमित्र’ श्रम ही आधार, सिर्फ खबरों से सरोकार। के तर्ज पर प्रकाशित होने वाला ऐसा समचाार पत्र है जो वर्ष 1978 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जैसे सुविधाविहीन शहर से स्व0 समूह सम्पादक कैलाशनाथ के श्रम के बदौलत प्रकाशित होकर आज पांच प्रदेश (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड) तक अपनी पहुंच बना चुका है।
Related Posts
अपनी टिप्पणियां पोस्ट करें
Latest News
07 May 2025 08:13:05
भोपाल । केन्द्र सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश के पांच जिलों में आज (बुधवार) नागरिक सुरक्षा योजनाओं का अभ्यास...



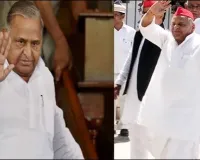








टिप्पणियां